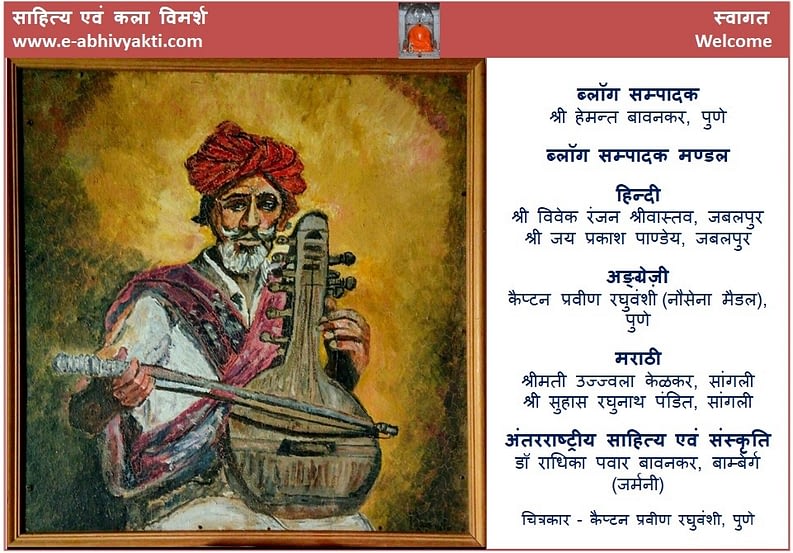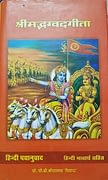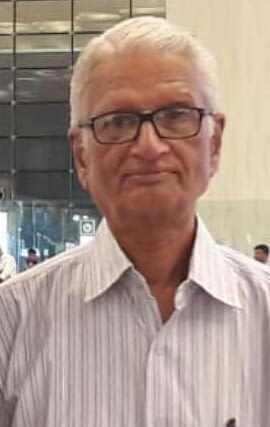सुश्री निशा नंदिनी भारतीय
(सुदूर उत्तर -पूर्व भारत की प्रख्यात लेखिका/कवियित्री सुश्री निशा नंदिनी जी के साप्ताहिक स्तम्भ – सामाजिक चेतना की अगली कड़ी में राजभाषा दिवस पर प्रस्तुत है हमारे उत्तर पूर्व में स्थित असम की आधिकारिक भाषा का ज्ञानवर्धक इतिहास असमिया भाषा का इतिहास।आप प्रत्येक सोमवार सुश्री निशा नंदिनी जी के साहित्य से रूबरू हो सकते हैं।)
☆ साप्ताहिक स्तम्भ – सामाजिक चेतना #65 ☆
☆ राजभाषा दिवस विशेष – असमिया भाषा का इतिहास ☆
आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की श्रृंखला में पूर्वी सीमा पर अवस्थित असम की भाषा को असमी,असमिया अथवा आसामीकहा जाता है।असमिया भारत के असम प्रांत की आधिकारिक भाषा तथा असम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। इसको बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक है।
भाषाई परिवार की दृष्टि से इसका संबंध आर्य भाषा परिवार से है। बांग्ला, मैथिली, उड़िया और नेपाली से इसका निकट का संबंध है। गियर्सन के वर्गीकरण की दृष्टि से यह बाहरी उपशाखा के पूर्वी समुदाय की भाषा है। सुनीतिकुमार चटर्जी के वर्गीकरण में प्राच्य समुदाय में इसका स्थान है। उड़िया तथा बंगला की भांति असमी की भी उत्पत्ति प्राकृत तथा अपभ्रंश से ही हुई है।
यद्यपि असमिया भाषा की उत्पत्ति सत्रहवीं शताब्दी से मानी जाती है। किंतु साहित्यिक अभिरुचियों का प्रदर्शन तेरहवीं शताब्दी में रुद्र कंदलि के द्रोण पर्व (महाभारत) तथा माधव कंदलि के रामायण से प्रारंभ हुआ। वैष्णवी आंदोलन ने प्रांतीय साहित्य को बल दिया।शंकर देव (1449-1567) ने अपनी लंबी जीवन-यात्रा में इस आंदोलन को स्वरचित काव्य, नाट्य व गीतों से जीवित रखा।
सीमा की दृष्टि से असमिया क्षेत्र के पश्चिम में बंगला है। अन्य दिशाओं में कई विभिन्न परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से तिब्बती, बर्मी तथा खासी प्रमुख हैं। इन सीमावर्ती भाषाओं का गहरा प्रभाव असमिया की मूल प्रकृति में देखा जा सकता है।असमिया एकमात्र बोली नहीं हैं। यह प्रमुखतः मैदानों की भाषा है।
बहुत दिनों तक असमिया को बंगला की एक उपबोली सिद्ध करने का उपक्रम होता रहा है। असमिया की तुलना में बंगला भाषा और साहित्य के बहुमुखी प्रसार को देखकर ही लोग इस प्रकार की धारण बनाते रहे हैं। परंतु भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से बंगला और असमिया का समानांतर विकास आसानी से देखा जा सकता है। मागधी अपभ्रंश के एक ही स्रोत से निःसृत होने के कारण दोनों में समानताएँ हो सकती हैं। पर उनके आधार पर एक दूसरे की बोली सिद्ध नहीं किया जा सकता।
क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से असमिया के कई उपरूप मिलते हैं। इनमें से दो मुख्य हैं- पूर्वी रूप और पश्चिमी रूप। साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से पूर्वी रूप को ही मानक माना जाता है। पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी रूप में बोलीगत विभिन्नताएँ अधिक हैं। असमिया के इन दो मुख्य रूपों में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्दसमूह, इन तीनों ही दृष्टियों से अंतर मिलते हैं। असमिया के शब्दसमूह में संस्कृत तत्सम, तद्भव तथा देशज के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। अनार्य भाषा परिवारों से गृहीत शब्दों की संख्या भी कम नहीं है। भाषा में सामान्यत: तद्भव शब्दों की प्रधानता है। हिंदी उर्दू के माध्यम से फारसी, अरबी तथा पुर्तगाली और कुछ अन्य यूरोपीय भाषाओं के भी शब्द आ गए हैं।
भारतीय आर्यभाषाओं की श्रृंखला में पूर्वी सीमा पर स्थित होने के कारण असमिया कई अनार्य भाषा परिवारों से घिरी हुई है। इस स्तर पर सीमावर्ती भाषा होने के कारण उसके शब्द समूह में अनार्य भाषाओं के कई स्रोतों के लिए हुए शब्द मिलते हैं। इन स्रोतों में से तीन अपेक्षाकृत अधिक मुख्य हैं-
(१) ऑस्ट्रो-एशियाटिक – खासी, कोलारी, मलायन
(२) तिब्बती-बर्मी-बोडो
(३) थाई-अहोम
शब्द समूह की इस मिश्रित स्थिति के प्रसंग में यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि खासी, बोडो तथा थाई तत्व तो असमिया में उधार लिए गए हैं। पर मलायन और कोलारी तत्वों का मिश्रण इन भाषाओं के मूलाधार के पास्परिक मिश्रण के फलस्वरूप है। अनार्य भाषाओं के प्रभाव को असम के अनेक स्थान नामों में भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिक, बोडो तथा अहोम के बहुत से स्थान नाम ग्रामों, नगरों तथा नदियों के नामकरण की पृष्ठभूमि में मिलते हैं। अहोम के स्थान नाम प्रमुखत: नदियों को दिए गए नामों में हैं।
असमिया लिपि मूलत: ब्राह्मी का ही एक विकसित रूप है। बंगला से उसकी निकट समानता है। लिपि का प्राचीनतम उपलब्ध रूप भास्कर वर्मन का 610 ई. का ताम्रपत्र है। परंतु उसके बाद से आधुनिक रूप तक लिपि में “नागरी” के माध्यम से कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं।
असमिया भाषा का व्यवस्थित रूप 13वीं तथा 14वीं शताब्दी से मिलने पर भी उसका पूर्वरूप बौद्ध सिद्धों के “चर्यापद” में देखा जा सकता है। “चर्यापद” का समय विद्वानों ने ईसवी सन् 600 से 1000 के बीच स्थिर किया है। दोहों के लेखक सिद्धों में से कुछ का तो कामरूप प्रदेश से घनिष्ट संबंध था। “चर्यापद” के समय से 12वीं शताब्दी तक असमी भाषा में कई प्रकार के मौखिक साहित्य का सृजन हुआ था। मणिकोंवर-फुलकोंवर-गीत, डाकवचन, तंत्र मंत्र आदि इस मौखिक साहिय के कुछ रूप हैं।
असमिया भाषा का पूर्ववर्ती रूप अपभ्रंश मिश्रित बोली से भिन्न रूप प्राय: 18वीं शताब्दी से स्पष्ट होता है। भाषागत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए असमिया के विकास के तीन काल माने जा सकते हैं।
14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के अंत तक। इस काल को फिर दो युगों में विभक्त किया जा सकता है। पहला वैष्णव-पूर्व युग दूसरा वैष्णव युग। इस युग के सभी लेखकों में भाषा का अपना स्वाभाविक रूप निखर आया है। यद्यपि कुछ प्राचीन प्रभावों से वह सर्वथा मुक्त नहीं हो सकी है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में पर्याप्त एकरूपता नहीं मिलती। परंतु असमिया के प्रथम महत्वूपर्ण लेखक शंकरदेव (जन्म-1449) की भाषा में ये त्रुटियाँ नहीं मिलती हैं। वैष्णव-पूर्व-युग की भाषा की अव्यवस्था यहाँ समाप्त हो जाती है। शंकरदेव की रचनाओं में ब्रजबुलि प्रयोगों का बाहुल्य है।
17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। इस युग में अहोम राजाओं के दरबार की गद्यभाषा का रूप प्रधान है। इन गद्य कर्ताओं को बुरंजी कहा गया है। बुरंजी साहित्य में इतिहास लेखन की प्रारंभिक स्थिति के दर्शन होते हैं। प्रवृत्ति की दृष्टि से यह पूर्ववर्ती धार्मिक साहित्य से भिन्न है। बुरंजियों की भाषा आधुनिक रूप के अधिक निकट है।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ से। 1819 ई. में अमरीकी बप्तिस्त पादरियों द्वारा प्रकाशित असमीया गद्य में बाइबिल के अनुवाद से आधुनिक असमीया का काल प्रारंभ होता है। मिशन का केंद्र पूर्वी आसाम में होने के कारण उसकी भाषा में पूर्वी आसाम की बोली को ही आधार माना गया। 1846 ई. में मिशन द्वारा एक मासिक पत्र “अरुणोदय” प्रकाशित किया गया। 1848 में असमीया का प्रथम व्याकरण छपा और 1867 में प्रथम असमीया अंग्रेजी शब्दकोश तैयार हुआ। श्रीमन्त शंकरदेव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा हिन्दू समाज सुधारक थे।
असमीया की पारंपरिक कविता उच्चवर्ग तक ही सीमित थी। भट्टदेव (1558-1638) ने असमिया गद्य साहित्य को सुगठित रूप प्रदान किया। दामोदरदेव ने प्रमुख जीवनियाँ लिखीं। पुरुषोत्तम ठाकुर ने व्याकरण पर काम किया। अठारहवी शती के तीन दशक तक साहित्य में विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिए। उसके बाद चालीस वर्षों तक असमिया साहित्य पर बांग्ला का वर्चस्व बना रहा। असमिया को जीवन प्रदान करने में चन्द्र कुमार अग्रवाल (1858-1938), लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा (1867-1838) व हेमचन्द्र गोस्वामी (1872-1928) का योगदान रहा। असमीया में छायावादी आंदोलन छेड़ने वाली मासिक पत्रिका जोनाकी का प्रारंभ इन्हीं लोगों ने किया था। उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यासकार पद्मनाभ गोहाञिबरुवा और रजनीकान्त बरदलै ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। सामाजिक उपन्यास के क्षेत्र में देवाचन्द्र तालुकदार व बीना बरुवा का नाम प्रमुखता से आता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य को मृत्यंजय उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस भाषा में क्षेत्रीय व जीवनी रूप में भी बहुत से उपन्यास लिखे गए हैं। 40वें व 50वें दशक की कविताएँ व गद्य मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित दिखाई देती है।
अहोम वंश की मुद्रा जिस पर असमिया लिपि में लिखा गया है। असमिया लिपि ‘पूर्वी नागरी’ का एक रूप है जो असमिया के साथ-साथ बांग्ला और विष्णुपुरिया मणिपुरी को लिखने के लिये प्रयोग की जाती है। केवल तीन वर्णों को छोड़कर शेष सभी वर्ण बांग्ला में भी ज्यों-के-त्यों प्रयुक्त होते हैं। ये तीन वर्ण हैं- ৰ (र), ৱ (व) और ক্ষ (क्ष)।
इस तरह असमिया भाषा का इतिहास बहुत प्राचीन और विस्तृत है।
© निशा नंदिनी भारतीय
9435533394
≈ ब्लॉग संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडल (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’/श्री जय प्रकाश पाण्डेय ≈