(श्री संजय भारद्वाज जी – एक गंभीर व्यक्तित्व । जितना गहन अध्ययन उतना ही गंभीर लेखन। शब्दशिल्प इतना अद्भुत कि उनका पठन ही शब्दों – वाक्यों का आत्मसात हो जाना है।साहित्य उतना ही गंभीर है जितना उनका चिंतन और उतना ही उनका स्वभाव। संभवतः ये सभी शब्द आपस में संयोग रखते हैं और जीवन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। हम आपको प्रति रविवार उनके साप्ताहिक स्तम्भ – संजय उवाच शीर्षक के अंतर्गत उनकी चुनिन्दा रचनाएँ आप तक पहुँचा रहे हैं। सप्ताह के अन्य दिवसों पर आप उनके मनन चिंतन को संजय दृष्टि के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। )
☆ संजय दृष्टि ☆ राजभाषा दिवस विशेष – राष्ट्रभाषा : मनन-मंथन-मंतव्य ☆
(विकिबुक्स ने हिंदी भाषा सम्बंधी लेखों के संकलन में इस लेख को प्रथम क्रमांक पर रखा है। लेख का शीर्षक ही संकलन को भी दिया है।)
भाषा का प्रश्न समग्र है। भाषा अनुभूति को अभिव्यक्त करने का माध्यम भर नहीं है। भाषा सभ्यता को संस्कारित करने वाली वीणा एवं संस्कृति को शब्द देनेवाली वाणी है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति नष्ट करनी हो तो उसकी भाषा नष्ट कर दीजिए। इस सूत्र को भारत पर शासन करने वाले विदेशियों ने भली भाँति समझा। आरंभिक आक्रमणकारियों ने संस्कृत जैसी समृद्ध और संस्कृतिवाणी को हाशिए पर कर अपने-अपने इलाके की भाषाएँ लादने की कोशिश की। बाद में सभ्यता की खाल ओढ़कर अंग्रेज आया। उसने दूरगामी नीति के तहत भारतीय भाषाओं की धज्जियाँ उड़ाकर अपनी भाषा और अपना हित लाद दिया। लद्दू खच्चर की तरह हिंदुस्तानी उसकी भाषा को ढोता रहा। अंकुश विदेशियों के हाथ में होने के कारण वह असहाय था।
यहाँ तक तो ठीक था। शासक विदेशी था, उसकी सोच और कृति में परिलक्षित स्वार्थ व धूर्तता उसकी कूटनीति और स्वार्थ के अनुरूप थीं। असली मुद्दा है स्वाधीनता के बाद का। अंग्रेजी और अंग्रेजियत को ढोते लद्दू खच्चरों की उम्मीदें जाग उठीं। जिन्हें वे अपना मानते थे, अंकुश उनके हाथ में आ चुका था किंतुु वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि अंतर केवल चमड़ी के रंग में हुआ था। देसी चमड़ी में अंकुश हाथ में लिए फिरंगी अब भी खच्चर पर लदा रहा। अलबत्ता आरंभ में पंद्रह बरस बाद बोझ उतारने का ‘लॉलीपॉप’ जरुर दिया गया। धीरे-धीरे ‘लॉलीपॉप’ भी बंद हो गया। खच्चर मरियल और मरियल होता गया।
राष्ट्रभाषा को स्थान दिये बिना राष्ट्र के अस्तित्व और सांस्कृतिक अस्मिता को परिभाषित करने की चौपटराजा प्रवृत्ति के परिणाम भी विस्फोटक रहे हैं। इन परिणामों की तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव की जा सकती है। इनमें से कुछ की चर्चा यहाँ की जा रही है।
राष्ट्रभाषा शब्द के तकनीकी उलझाव और आठवीं अनुसूची से लेकर अपभ्रंश बोलियों तक को राष्ट्रभाषा की चौखट में शामिल करने के शाब्दिक छलावे की चर्चा यहाँ अप्रासंगिक है। राष्ट्रभाषा से स्पष्ट तात्पर्य देश के सबसे बड़े भूभाग पर बोली-लिखी और समझी जाने वाली भाषा से है। भाषा जो उस भूभाग पर रहनेवाले लोगों की संस़्कृति के तत्वों को अंतर्निहित करने की क्षमता रखती हो, जिसमें प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों से शब्दों के आदान-प्रदान की उदारता निहित हो। हिंदी को उसका संविधान प्रदत्त पद व्यवहारिक रूप में प्रदान करने के लिए आम सहमति की बात करने वाले भूल जाते हैं कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाषा अनेक नहीं होते। हिंदी का विरोध करने वाले कल यदि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत पर भी विरोध जताने लगें, अपने-अपने ध्वज फहराने लगें, गीत गाने लगें तो क्या कोई अनुसूची बनाकर उसमें कई ध्वज और अनेक गीत प्रतिष्ठित कर दिये जायेंगे? क्या तब भी यह कहा जायेगा कि अपेक्षित राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज आम सहमति की प्रतीक्षा में हैं? भीरु व दिशाहीन मानसिकता दुःशासन का कारक बनती है जबकि सुशासन स्पष्ट नीति और पुरुषार्थ के कंधों पर टिका होता है।
सांस्कृतिक अवमूल्यन का बड़ा कारण विदेशी भाषा में देसी साहित्य पढ़ाने की अधकचरी सोच है। राजधानी के एक अंग्रेजी विद्यालय ने पढ़ाया गया- ‘सीता वॉज़ स्वीटहार्ट ऑफ रामा।’ ठीक इसके विपरीत श्रीराम को सीताजी के कानन-कुण्डल मिलने पर पहचान के लिए लक्ष्मण जी को दिखाने का प्रसंग स्मरण कीजिए। लक्ष्मण जी का कहना कि मैने सदैव भाभी माँ के चरण निहारे, अतएव कानन-कुण्डल की पहचान मुझे कैसे होगी?- यह भाव संस्कृति की आत्मा है। कुसुमाग्रज की मराठी कविता में शादीशुदा बेटी का मायके में ‘चार भिंतीत नाचली’ ( शादीशुदा बेटी का मायके आने पर आनंद विभोर होना) का भाव तलाशने के लिए सारा यूरोपियन भाषाशास्त्र खंगाल डालिये। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।
कटु सत्य यह है कि भाषाई प्रतिबद्धता और सांस्कृतिक चेतना के धरातल पर वर्तमान में भयावह उदासीनता दिखाई देती है। समृद्ध परंपराओं के स्वर्णमहल खंडहर हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम से बेदखल किया जाना। चूँकि भाषा संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन यूरोपीय संस्कृति का आयात कर रहा है। एक भव्य धरोहर डकारी जा रही है और हम दर्शक-से खड़े हैं। शिक्षा के माध्यम को लेकर बनी शिक्षाशास्त्रियों की अधिकांश समितियों ने सदा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने की सिफारिश की। यह सिफारिशें वर्षों कूड़े-दानों में पड़ी रहीं। नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने पहली बार प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने को प्रधानता दी है। यह सराहनीय है।
यूरोपीय भाषा समूह की अंग्रेजी के प्रयोग से ‘कॉन्वेंट एजुकेटेड’ पीढ़ी, भारतीय भाषा समूह के अनेक अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाती। ‘ड़’,‘ण’ अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। ‘पूर्ण’, पूर्न हो चला है, ‘ शर्म ’ और ‘श्रम’ में एकाकार हो चला है। हृस्व और दीर्घ मात्राओं के अंतर का निरंतर होता क्षय अर्थ का अनर्थ कर रहा है।‘लुटना’ और ‘लूटना’ एक ही हो गये हैं। विदेशियों द्वारा की गई ‘लूट’ को ‘लुटना’ मानकर हम अपनी लुटिया डुबोने में अभिभूत हो रहे हैं।
लिपि नये संकट से गुजर रही है। इंटरनेट पर खास तौर पर फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर जैसी साइट्स पर देवनागरी को रोमन में लिखा जा रहा है। ‘बड़बड़’ के लिए barbar/ badbad (बर्बर या बारबर या बार-बार) लिखा जा रहा है। ‘करता’, ‘कराता’, ‘कर्ता’ में फर्क कर पाना भी संभव नहीं रहा है। जैसे-जैसे पीढ़ी पेपरलेस हो रही है, स्क्रिप्टलेस भी होती जा रही है। मृत्यु की अपरिहार्यता को लिपि पर लागू करनेवाले भूल जाते हैं कि मृत्यु प्राकृतिक हो तब भी प्राण बचाने की चेष्टा की जाती है। ऐसे लोगों को याद दिलाया जाना चाहिये कि यहाँ तो लिपि की सुनियोजित हत्या हो रही है और हत्या के लिए भारतीय दंडसंहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान है।
सारी विसंगतियों के बीच अपना प्रभामंडल बढ़ाती भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के विरुद्ध ‘फूट डालो और राज करो’ की कूटनीति निरंतर प्रयोग में लाई जा रही है। इन दिनों हिंदी की बोलियों को स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता दिलाने की गलाकाट प्रतियोगिता शुरु हो चुकी है। खास तौर पर गत जनगणना के समय इंटरनेट के जरिये इस बात का जोरदार प्रचार किया गया कि हम हिंदी की बजाय उसकी बोलियों को अपनी मातृभाषा के रूप में पंजीकृत करायें। संबंधित बोली को आठवीं अनुसूची में दर्ज कराने के सब्जबाग दिखाकर, हिंदी की व्यापकता को कागज़ों पर कम दिखाकर आंकड़ो के युद्ध में उसे परास्त करने के वीभत्स षड्यंत्र से क्या हम लोग अनजान हैं? राजनीतिक इच्छाओं की नाव पर सवार बोलियों को भाषा में बदलने के आंदोलनों के प्रणेताओं (!) को समझना होगा कि यह नाव उन्हें घातक भाषाई षड्यंत्र की सुनामी के केंद्र की ओर ले जा रही है। अपनी राजनीति चमकाने और अपनी रोटी सेंकनेवालों के हाथ फंसा नागरिक संभवतः समझ नहीं पा रहा है कि यह भाषाई बंदरबाँट है। रोटी किसीके हिस्से आने की बजाय बंदर के पेट में जायेगी। बेहतर होता कि मूलभाषा-हिंदी और उपभाषा के रूप में बोली की बात की जाती।
संसर्गजन्य संवेदनहीनता, थोथे दंभवाला कृत्रिम मनुष्य तैयार कर रही है। कृत्रिमता की ये पराकाष्ठा है कि मातृभाषा या हिंदी न बोल पाने पर व्यक्ति लज्जा अनुभव नहीं करता पर अंग्रेजी न जानने पर उसकी आँखें स्वयंमेव नीची हो जाती हैं। शर्म से गड़ी इन आँखों को देखकर मैकाले और उसके भारतीय वंशजों की आँखों में विजय के अभिमान का जो भाव उठता होगा, ग्यारह अक्षौहिणी सेना को परास्त कर वैसा भाव पांडवों की आँखों में भी न उठा होगा।
संस्कृत को पाठ्यक्रम से हटाना एक अक्षम्य भूल रही। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी, प्रादेशिक भाषा एवं संस्कृत/अन्य क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान किया जाता तो देश को ये दुर्दिन देखने को नहीं मिलते। अब तो हिंदी को पालतू पशु की तरह दोहन मात्र का साधन बना लिया गया है। जनता से हिंदी में मतों की याचना करनेवाले निर्वाचित होने के बाद अधिकार भाव से अंग्रेजी में शपथ उठाते हैं।
साहित्यकारों के साथ भी समस्या है। दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के बड़े वर्ग में भाषाई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं देती। इनमें से अधिकांश ने भाषा को साधन बनाया, साध्य नहीं। यही स्थिति हिंदी की रोटी खानेवाले प्राध्यापकों, अधिकारियों और हिंदी फिल्म के कलाकारों की भी है। सिनेमा में हिंदी में संवाद बोलकर हिंदी की रोटी खानेवाले सार्वजनिक वक्तव्य अंग्रेजी में करते हैं। ऐसे सारे वर्गों के लिए वर्तमान दुर्दशा पर अनिवार्य आत्मपरीक्षण का समय आ चुका है।
भाषा के साथ-साथ भारतीयता के विनाश का जो षडयंत्र रचा गया, वह अब आकार ले चुका है। भारत में दी जा रही तथाकथित आधुनिक शिक्षा में रोल मॉडेल भी यूरोपीय चेहरे ही हैं। नया भारतीय अन्वेषण अपवादस्वरूप ही दिखता है। डूबते सूरज के भूखंड से आती हवाएँ, उगते सूरज की भूमि को उष्माहीन कर रही हैं।
छोटी-छोटी बात पर और प्रायः बेबात संविधान को इत्थमभूत धर्मग्रंथ-सा मानकर अशोभनीय व्यवहार करने वाले छुटभैयों से लेकर कथित राष्ट्रीय नेताओं तक ने कभी राष्ट्रभाषा को मुद्दा नहीं बनाया। जब कभी किसीने इस पर आवाज़ उठाई तो बरगलाया गया कि भाषा संवेदनशील मुद्दा है। तो क्या देश को संवेदनहीन समाज अपेक्षित है? कतिपय बुद्धिजीवी भाषा को कोरी भावुकता मानते हैं। शायद वे भूल जाते हैं कि युद्ध भी कोरी भावुकता पर ही लड़ा जाता है। युद्धक्षेत्र में ‘हर-हर महादेव’ और ‘पीरबाबा सलामत रहें’ जैसे भावुक (!!!) नारे ही प्रेरक शक्ति का काम करते हैं। यदि भावुकता से राष्ट्र एक सूत्र में बंधता हो, व्यवस्था शासन की दासता से मुक्त होती हो, शासकों की संकीर्णता पर प्रतिबंध लगता हो, अनुशासित समाज जन्म लेता हो तो भावुकता देश की अनिवार्य आवश्यकता हो जाती है।
हिंदी पखवाड़े के किसी एक दिन हिंदी के नाम का तर्पण कर देने या सरकारी सहभोज में सम्म्मिलित हो जाने भर से हिंदी के प्रति भारतीय नागरिक के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो सकती। आवश्यक है कि नागरिक अपने भाषाई अधिकार के प्रति जागरुक हों। वे सूचना के अधिकार के तहत राष्ट्रभाषा को राष्ट्र भर में मुद्दा बनाएँ।
भारतीय भाषाओं के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए छात्रों से अपेक्षित है कि वे अपनी भाषा में उच्च शिक्षा पाने के अधिकार को यथार्थ में बदलने के लिए पहल करें। स्वाधीनता के सत्तर वर्ष बाद भी न्यायव्यवस्था के निर्णय विदेशी भाषा में आते हों तो संविधान की पंक्ति-‘भारत एक सार्वभौम गणतंत्र है’ अपना अर्थ खोने लगती है।
भारतीय युवाओं से वांछित है कि दुनिया की हर तकनीक को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करा दें। आधुनिक तकनीक और संचार के अधुनातन साधनों से अपनी बात दुनिया तक पहुँचाना तुलनात्मक रूप से बेहद आसान हो गया है। भारतीय भाषाओं में अंतरजाल पर इतनी सामग्री अपलोड कर दें कि ज्ञान के इस महासागर में डुबकी लगाने के लिए अन्य भाषा भाषी भी हमारी भाषाएँ सीखने को विवश हो जाएँ।
सरकार से अपेक्षित है कि हिंदी प्रचार संस्थाओं के सहयोग से विदेशियों को हिंदी सिखाने के लिए क्रैश कोर्सेस शुरू करे। भारत आनेवाले सैलानियों के लिए ये कोर्सेस अनिवार्य हों। वीसा के लिए आवश्यक नियमावली में इसे समाविष्ट किया जा सकता है।
बढ़ते विदेशी पूँजीनिवेश के साथ भारतीय भाषाओं और भारतीयता का संघर्ष ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’की स्थिति में आ खड़ा हुआ है। समय की मांग है कि हिंदी और सभी भारतीय भाषाएँ एकसाथ आएँ। प्रादेशिक स्तर पर प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के नारे को बुलंद करना होगा। ‘अंधाधुंध अंग्रेजी’के विरुद्ध ये एकता अनिवार्य है।
बीते सात दशकों में पहली बार भाषा नीति को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार संवेदनशील और सक्रिय दिखाई दे रही है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता, भारत और भारतीयता के पक्ष में स्वयं प्रधानमंत्री ने पहल की है। मंत्री तो मंत्री रक्षा और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी हिंदी में अपनी बात रख रहे हैं। नई शिक्षानीति भारतीय भाषाओं की उन्नति की दृष्टि से दूरगामी सिद्ध होगी। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो,च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो या उच्चस्तर पर आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन, अरुणोदय की संभावनाएँ तो बन रही हैं। आशा है कि इन किरणों के आलोक में ‘इंडिया’की केंचुली उतारकर ‘भारत’ शीघ्रतिशीघ्र बाहर आएगा।

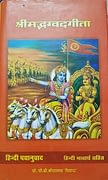

 लेखनी सुमित्र की – दोहे ..संदर्भ हिंदी
लेखनी सुमित्र की – दोहे ..संदर्भ हिंदी 










