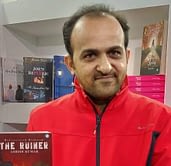श्री सूबेदार पाण्डेय “आत्मानंद”
(आज प्रस्तुत है श्री सूबेदार पाण्डेय “आत्मानंद” जी द्वारा रचित शब्दों के सामर्थ्य पर आधारित आलेख “शब्द सामर्थ्य ”।)
☆ शब्द सामर्थ्य ☆
भाषा व्याकरण की दृष्टि से देखा जाये तो ज्ञात होताहै, कि अक्षरों के समूह से शब्द बनते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग भाषा लिपि की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। वाक्य रचना, तथा काव्य रचना में उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार एकही शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त होते हैं। नीचे उदाहरण से लेखक के मन्तव्यों को समझें।
दोहा—-
चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिउ ओर।
सुबरन को खोजत फिरत, कवि, ब्यभिचारी, चोर।।
यहां सुबरन का अर्थ कवि के लिए सुन्दर वर्ण, व्याभिचारी के लिए सुन्दर स्त्री, तथा चोर के अर्थ में सोना है।
अथवा
रहिमन पानी राखिये, बिनु पानी सब सून।
पानी गये न उबरे, मोती मानुष चून।
यहां पानी शब्द का प्रयोग, मोती मानुष चून (पक्षी) के लिए किया गया है जो अलग अलग परिपेक्ष में है। इस प्रकार परिस्थिति जन्य परिपेक्ष की आवश्यकता अनुसार शब्दों के अर्थ तथा। भाव बदलते ही रहते हैं। शब्द ही साहित्य विधा के लेखन की प्राण चेतना है।
शब्द ही हृदय के भावों एवं मन के विचारों का प्रस्तोता (प्रस्तुत ) करने वाला है। साहित्यिक विधा में शब्दों से अलंकारिक भाषा का सौन्दर्य बोध, रस छंद अलंकार के सुन्दर भावों की उत्पत्ति होती है। शब्दों में ही मंत्रो की शक्ति बसती है। जिनके विधि पूर्वक अनवरत जाप के बड़े चमत्कृत कर देने वाले परिणाम देखे गये हैं। और निर्धारित उद्देश्यो की सफलता भी।
शब्दों का प्रभाव सीधे सीधे मन मस्तिष्क तथा हृदय पर होता है। शब्दों से ही दुख के समय संवेदना, सुख के समय प्रसन्नता, तथा आक्रोश के समय में क्रोध प्रकट होताहै। जो हजारों किलोमीटर बैठे। मानव के मन को सुख दुःख पीड़ा का एहसास करा जाता है, इसका अनुभव मुझे आपको तथा सभी को होगा। तथा वे शब्द ही तो है जो सामनेवाले के आचार विचार तथा व्यवहार पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कहा भी गया है कि गोली के घाव तो भर जाते हैं, बोली के घाव जो शब्दों से मिलते हैं वो जल्दी नहीं भरते।
शब्दों से ही स्तुति गान प्रशस्तिगान है क्योंकि उसमें बहुत जान है। शब्द ही बोलचाल भाषा तथा अभिव्यक्ति के माध्यम के मूलाधार है। वाणी से शब्द प्राकट्य तथा लेखन से उसका स्वरूप बनता है।
तभी तो श्री कबीर साहेब कहते हैं—–
ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोय।
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय।।
और इन्हीं भावों के समर्थन में वाणी की महत्ता बताते हुए श्री तुलसी दास जी कह उठते हैं—–
तुलसी मीठे बचन ते, सुख उपजै चंहुओर।
मधुर बचन इक मंत्र है, तजि दे बचन कठोर।।
इस प्रकार मधुर शब्दों से सराबोर वाणी जो मंत्र सा चमत्कारिक प्रभाव छोड़ती है। और सामने वाले को अपने प्रभाव मे ले लेती है।
ऐसे अनुभव आप सभी के पास होंगे जहां कठोर वाणी। अपनो से भी दूर कर देती है, वही मृदु वाणी सबको ही अपना बना लेती है।
शब्दों में समाये भावों का बड़ा ही सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मेरे अपने विचारों से शब्द ही भाषा ,भाव व वाणी के मूल श्रोत है तो साहित्य सृजन के सौन्दर्य बोध भी। जहाँ अक्षर शब्दो के जनक है, तो शब्द ही गीत संगीत विधा के माधुर्य भी, जिसके सम्मोहन से आदमी तो क्या जानवर भी नहीं बचते। ऐसा पौराणिक कथाओं में मिलता है जब कृष्ण की बांसुरी ने सबके मन को मोहा था।
अपनी गरिमा मय प्रभाव एवं स्वभाव से शब्द प्रतिपल मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। शब्दकोश बढ़ने से ही मानव कवि, लेखक, रचनाकार, पत्रकार बन जाता है। तथा आदर्श अभिव्यक्ति कर भावों का चितेरा बन जाता है।
बिना अक्षरों के ज्ञान के भी शब्द ज्ञान संभव है, तभी तो बिना पढ़े लिखे छोटे बच्चे भी तो अपनी भाषा में बात कर पाते हैं। अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान प्राथमिक पाठशाला के प्रथम कक्षा के छात्रों की नींव की ईंट है। प्रत्येक शब्द में असीम सामर्थ्य है।
-सुबेदार पांडेय “आत्मानंद”
संपर्क – ग्राम जमसार, सिंधोरा बाज़ार, वाराणसी – 221208
मोबा—6387407266