श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’
(हम प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’जी के आभारी हैं जो साप्ताहिक स्तम्भ – “विवेक की पुस्तक चर्चा” शीर्षक के माध्यम से हमें अविराम पुस्तक चर्चा प्रकाशनार्थ साझा कर रहे हैं । श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र जी, मुख्यअभियंता सिविल (म प्र पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी, जबलपुर ) पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तकनीकी पृष्ठभूमि के साथ ही उन्हें साहित्यिक अभिरुचि विरासत में मिली है। उनका दैनंदिन जीवन एवं साहित्य में अद्भुत सामंजस्य अनुकरणीय है। इस स्तम्भ के अंतर्गत हम उनके द्वारा की गई पुस्तक समीक्षाएं/पुस्तक चर्चा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
आज प्रस्तुत है आपके द्वारा श्री कुमार सुरेश द्वारा लिखित पुस्तक “संभावामि युगे युगे” (जीवनी) पर चर्चा।
☆ साप्ताहिक स्तम्भ – विवेक की पुस्तक चर्चा# 165 ☆
☆ “संभवामि युगे युगे” – लेखक … श्री कुमार सुरेश ☆ चर्चा – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’ ☆
पुस्तक चर्चा
संभवामि युगे युगे
आई एस बी एन ९७८.९३.८९४७१.५०.२
कुमार सुरेश
विद्या विहार नई दिल्ली
मूल्य ३०० रु
चर्चा …. विवेक रंजन श्रीवास्तव
मो ७०००३७५७९८
श्रीमद्भगवत गीता के चौथे अध्याय के आठवें श्लोक “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ “से श्री कुमार सुरेश ने किताब का शीर्षक लिया है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि दुष्टों के विनाश के लिये मैं हर युग में हर युग में फिर फिर जन्म लेता हूं। विदेशी आक्रांताओ के विरुद्ध भारत की निरंतर संघर्ष गाथा का इससे बेहतर शीर्षक भला हो भी क्या सकता था। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सारा जहाँ हमारा। प्रगति के लिये अस्तित्व का यह संघर्ष रूप बदल बदल कर फिर फिर हमारे समाज में खड़ा होता रहा है, आज भी जारी ही है। कुमार सुरेश मूलतः एक अध्येता और विचारक बहुविध लेखक हैं। कभी उनका व्यंग्यकार उनसे तंत्रकथा जैसा मारक व्यंग्य उपन्यास लिखवा डालता है, तो कभी वे व्यंग्यराग लिखते हैं जिसमें वे अपने स्फुट व्यंग्य संग्रहित कर साहित्य जगत को सौंपते हैं। कभी उनके अंदर का कवि “शब्द तुम कहो”, “भाषा सांस लेती है”, “आवाज एक पुल है ” जैसी कविताओ के महत्वपूर्ण संग्रह रच देता है। साहित्य जगत उन्हें गंभीरता से पढ़ता और रजा पुरस्कार या शरद जोशी जैसे सम्मानो से सम्मानित करता है। कुमार सुरेश के पास अनुभव है, उन्होंने प्रकाशन जगत में भी दस्तक दी थी, वे प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। उनके पास जन सामान्य पाठक तक पहुंचने वाली अभिव्यक्ति और भाषा सामर्थ्य है। वे मेरे अभिन्न सारस्वत मित्र हैं, और इस किताब की लेखन यात्रा में पाण्डुलिपि पढ़ने, शीर्षक तय करने तथा प्रकाशक कौन हो यह निर्णय लेने में पल पल अवगत रहने का गौरव मुझे रहा है।
अपने इतिहास को जानना समझना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इतिहास के प्रति जिज्ञासा नैसर्गिक मनोवृत्ति होती है। घर परिवार कुटुम्ब में दादियों की ज्वैलरी के डिब्बे में सिजरे होते हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी खानदान का हाल नाम पते मिल जाते हैं। जिनके घरों में यह नहीं उनकी पुश्तों का हिसाब प्रयाग संगम के पंडो के पास मिल ही जाता है। राजस्थान में वंशावली लेखन की परंपरा है। पुराने राजाओ ने अपने दरबार में इस कार्य के लिये लोगों को रखा था, जो बढ़ा चढ़ा कर राजाओ तथा उनके पूर्वजों और राज परिवार के सदस्यों की वीरता तथा महिलाओ की सुंदरता के किस्से लिखा करते थे। यह वंशावली लेखन की व्यवस्था आज भी राजस्थान में चल रही है। गौरव शाली इतिहास पर नई पीढ़ी गर्व करती है, पुरानी गलतियों से शिक्षा लेती है किंतु यह भी सही है कि इतिहास का ज्ञान वर्तमान में कटुता भी फैलाता है, आज देश में यही देखने में आ रहा है। राजनैतिक दल इसका लाभ लेने से बाज नहीं आ रहे। अस्तु।
संभवामि युगे युगे में कुमार सुरेश ने कालक्रम में प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर संदर्भ देते हुये सिकंदर के समय से औरंगजेब के काल तक भारतीय इतिहास को अपनी वांछित तीप के साथ संजोने में सफलता अर्जित की है। पुस्तक के अध्यायों का अवलोकन करें तो पुस्तक लेखन का मूल आशय समझ आ जाता है। वर्तमान में जो इतिहास पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है, उसमें अनेक विदेशी आक्रांताओ का महिमा मंडन पढ़ने मिलता है। संभवतः गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति बताकर उन आक्रांताओ का पक्ष सशक्त होने के चलते सामाजिक समरसता बनाये रखने के लिये वामपंथी इतिहास कारों ने ऐसा किया। किन्तु कुमार सुरेश ने पूरी ढ़ृड़ता से ऐसे कई आक्रांताओ की क्रूरता और अत्याचार पर बेबाकी से लिखा है। उन्होंने यह धारणा भी खंडित की है कि समुचा भारतवर्ष पर मुगल साम्राज्य के अधीन था।
पहले अध्याय “भारत सदा से एक राष्ट्र है”, में लेखक ने आर्य संस्कृति को मूलतः भारतीय संस्कृति लिखते हुये हिन्दुओ के देश भर में फैले ज्योतिर्लिंग, देवी पीठों, कुंभ के आयोजनो जैसे तर्क रोचक तरीके से रखा है। पुस्तक में डी एन ए एनालिसिस के वैज्ञानिक आधार पर आर्य तथा द्रविड़ को मूलतः भारत का हिस्सा बताया गया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि १९४६ में ही अंबेडकर जी ने सिद्ध कर दिया था कि आर्य बाहर से नहीं आये थे। दूसरा अध्याय “सोने की चिड़िया पर बुरी नजरें ” है। किंचित भारतीय भूगोल, भारत से जुड़ने वाले विदेशी मार्गों के सचित्र वर्णन के साथ अखण्ड भारत की तत्कालीन संपन्नता और इस वजह से विदेशियों की भारत में रुचि पर विशद वर्णन इस अध्याय में है। इस पुस्तक को लिखने के लिये लम्बे समय तक कुमार सुरेश ने गहन अध्ययन किया है, जिनमें दर्जन भर से अधिक अंग्रेजी की किताबें हैं जिन्हें अध्ययन कर उनके वांछित कथ्य अपने तर्क रखने के लिये लेखक ने किया है। यह तथ्य संदर्भांकित पुस्तकों की सूची ही नहीं हर अध्याय में उधृत एतिहासिक अंश स्पष्ट करते हैं। जब सिकंदर आता है कोई पोरुष खड़ा हो जाता है, प्रतिरोध की यह भारतीय मूल प्रवृति ही संभवामि युगे युगे है जिसके चलते आज भी भारत अपनी मूल संस्कृति के साथ यथावत दुनियां में विश्वगुरू बना खड़ा हुआ है। चौथा अध्याय ” सिंध पर अरबों का आक्रमण उनके लिये एक न भूलने वाली असफलता बन गया ” है। भारतीय योद्धाओं ने अधिकांशतः कभी स्वयं किसी पर आक्रमण भले न किया हो पर हमेशा आक्रांताओ के प्रतिरोध में सुनिश्चित हार के खतरे को भांपते हुए भी हमेशा आक्रांताओं का मुकाबला पूरी वीरता और साहस से किया। इतिहास के बड़े-बड़े कालखंड ऐसे थे, जिनमें विदेशी आक्रांताओं को पराजय मिली। ये कालखंड छोटे नहीं, तीन सौ सालों तक लंबे रहे हैं। भारत में अनेक हिस्से ऐसे हैं, जिनमें आक्रांता कभी प्रवेश नहीं कर पाए। आक्रमणकारियों को सदैव भारत पर आक्रमण की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बीच में ऐसे काल भी आए, जब विदेशी आक्रांताओं को कुछ सफलता मिली। किंतु जैसे ही मौका मिला, कोई-न-कोई वीर उठकर खड़ा हो गया। किसी-न-किसी क्षेत्र के आम लोगों ने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष किया और उसे पराजित किया या इतना नुकसान तो जरूर पहुँचाया कि आक्रांता को भारतीय इच्छाओं का आदर करना पड़ा। भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की ऊर्जा हमारे जिन पूर्वजों के बलिदानों से प्राप्त हुई है, यह पुस्तक उन पूर्वजों के प्रति लेखक की कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रयास है। आठवी सदी में इस्लाम के भौगोलिक विस्तार को नक्शों के जरिये बताया गया है। अगले अध्याय का नाम हिंदूशाही वंश का शौर्य है। जिसमें महमूद गजनी से राजस्थान के योद्धाओ की चर्चा है। मीर तकी मीर ने एक शेर लिखा था ” उसके फरोग हुस्न में झमके है सब में नूर ” जिसमें उन्होंने काबा और सोमनाथ को एक सृदश ही बताया था। महमूद गजनवी की सेना के लौटने से भारतीय समृद्धि की सूचनायें विदेशों तक पहुंची और इसके चलते भारत पर आक्रमण के तांते लग गये। छोटे छोटे अध्यायों में बिंदु रूप से बड़ी बातें कह देने में लेखक ने सफलता अर्जित की है। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से भारतीय इतिहास का गौरव है, उसे एक पूरे चेप्टर ” सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिन्हें केवल धोखे से हराया जा सका ” में लिखा गया है। पूर्वोत्तर से भी आक्रांताओ ने भारत पर हमले के प्रयास किये थे पर असम के वीरों ने बक्तियार खिलजी को ऐसी धूल चटाई कि हमेशा के लिये उस ओर से भारत पर विदेशी आक्रमण नियंत्रित बने रहे। भारतीय प्रतिरोध की खासियत पीढ़ी दर पीढ़ी आक्रांता सल्तनतों का विरोध रहा है। राजस्थान के वीरों की ही नहीं वहां की वीरांगनाओ द्वारा उठाये गये कदम अद्भुत रहे हैं। उन पर पूरा अध्याय लिखा गया है। जिस भारतीय संस्कृति की विशेषता ही यह है कि वह हमारी रगों में पल्लवित पोषित होती है। जहां भी भारतीय गये वहां उनके साथ भारतीयता भी गई। लेखक ने स्पष्ट किया है कि १४०० ई तक विदेशी आक्रांता समझ गये कि भारतीय संस्कृति को मिटाना असंभव है। बाबर के आक्रमण का प्रतिरोध, पानीपत की लड़ाई, हेमू का विस्मृत बलिदान, मुगलों को निरंतर चुनौती, औरंगजेब से जाट, मराठों और राजपूतों के संघर्ष, समुद्र के रास्ते पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स यूरोपियन्स के भारत प्रवेश, १८५७ के संग्राम से पहले भी अंग्रेजो को भारत से निकालने के प्रयास एक चेप्टर में प्रस्तुत किये गये हैं। अंतिम अध्याय है ” यह बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ” जिसमें लेखक ने अपने एतिहासिक अध्ययन का निचोड़ रख कर हमें गर्व का अवसर दिया है।
इतिहास की २०० से ज्यादा पृष्ठो पर फैली रोचक सामग्री को समेटना दुष्कर कार्य होता है। मैने पुस्तक की विषय वस्तु की बिन्दु रूप चर्चा कर किताब से पाठको को परिचित कराने का प्रयास किया है, किताब अमेजन सहित विभिन्न प्लेटफार्म पर उपलब्ध है, किताब बुलवाईये और पढ़िये तभी आप भारत के गौरवशाली इतिहास को लेखक के नजरिये से समझ सकेंगे। किताब पैसा वसूल तो है ही, संदर्भ के लिये संग्रहणीय है।
चर्चा …. विवेक रंजन श्रीवास्तव
चर्चाकार… विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’
समीक्षक, लेखक, व्यंगयकार
ए २३३, ओल्ड मीनाल रेसीडेंसी, भोपाल, ४६२०२३, मो ७०००३७५७९८
readerswriteback@gmail.कॉम, [email protected]
≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडल (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’/श्री जय प्रकाश पाण्डेय ≈

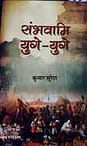



 संजय दृष्टि – समीक्षा का शुक्रवार # 6
संजय दृष्टि – समीक्षा का शुक्रवार # 6  सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध – लेखिका – सुश्री वीनु जमुआर
सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध – लेखिका – सुश्री वीनु जमुआर 











 पुस्तकावर बोलू काही
पुस्तकावर बोलू काही 




