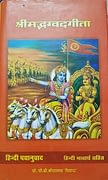डॉ. अनिता एस. कर्पूर ’अनु’

( ई- अभिव्यक्ति में डॉ. अनिता एस. कर्पूर ’अनु’ जी का हार्दिक स्वागत है। आप बेंगलुरु के जैन महाविद्यालय में सह प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं की सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिकता, स्वर्ण मुक्तावली- कविता संग्रह, स्पर्श – कहानी संग्रह, कशिश-कहानी संग्रह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त आपकी एक लम्बी कविता को इंडियन बुक ऑफ़ रिकार्ड्स 2020 में स्थान दिया गया है। आप कई विशिष्ट पुरस्कारों / अलंकरणों से पुरस्कृत / अलंकृत हैं। आज ससम्मान प्रस्तुत है आपकी एक बेहद खूबसूरत और संजीदा कहानी ज़मीन। जीवन के कई सत्य और पुरस्कारों के संसार की ज़मीन के सत्य को उजागर करती इस बेबाक कहानी के लिए डॉ. अनिता एस. कर्पूर ’अनु’ जी की लेखनी को सदर नमन।)
☆ कथा-कहानी ☆ ज़मीन ☆
चारु संमुदर के किनारे बैठकर अपनी बीती जिंदगी को याद कर रही है । चारु अपने यौवन में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी । उसके चेहरे पर तेज भी सूरज को कमज़ोर और चांद भी उसके सामने फीके पड जाते है । आप सोच नहीं सकते इतनी सुंदर थी । विश्वसुंदरी को भी मात देनेवाली एक लड़की चारु थी । उसके परिवार के लोगों ने उसे कभी भी विश्वसुंदरी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहायता नहीं की थी । उसका परिवार परंपरागत रुढिवादी से भरा था । उसके पिता जी की बात पूरे परिवार में चलती थी । चारु को कुछ भी काम होता तो वह पहले अपने पिताजी को मनाती थी । घर में पुरुष का वर्चस्व अधिक था । रमेश रोज सुबह पूजा करते थे । उसकी माँ चांदनी उनके लिए पूजा की सामग्री सब सजाकर रखती थी । एक दिन भी उनसे नहीं होता तो रमेश चिल्लाते थे । चारु को कॉलेज में आगे पढ़ना था ।
रमेश ने साफ मना कर दिया था कि अब आगे चारु पढाई नहीं करेगी । चांदनी मुझे लगता है कि उसे घर के काम सीखने चाहिए । उसे सारी औरतों के काम सीखा देना । अपना फैसला सुनाकर वे अपने ऑफिस के लिए निकल गए ।
उनके जाते ही चारु उनकी नकल करते हुए अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप इस इन्सान के साथ कैसे रह लेती हो? मेरे लिए कभी भी ऐसा पति मत ढूँढना । माँ मुझे आगे पढना है । आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे समाज में बहुत सारे काम करने है । आप बताइए माँ, क्या मैं घर की चाहरदीवारी में बैठकर चूल्हा चौका करने ही पैदा हुई हूँ ? आप बताइए । अगर ऐसा ही था तो मुझे पैदा ही क्यों किया ? माँ…माँ… बात क्यों नहीं कर रही हो, कहते हुए चारु अपनी माँ को ज़ोर से हिलाती है ।
चांदनी की आँखों में आंसू बह रहे थे । उसने आंसू पौंछाकर कहा, सही कहा तुमने । सबसे परे मैं माँ हूँ । मैं कैसे अपनी फूल सी बच्ची को किसी कसाई के हवाले कर देती, बताओ । बडी आई कहनेवाली कि मुझे मार दिया होता तो अच्छा होता कहनेवाली । तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो बिटिया । हाँ, मानती हूँ कि तुम्हारे पिताजी को लड़की पहले से पसंद नहीं है । वह हंमेशा लड़की को जिम्मेदारी ही समझते है । मतलब यह तो नहीं कि बच्ची को मार दिया जाय । रमेश डरते है कि उनकी सुंदर बच्ची पर किसीकी नज़र न पड़ जाय । उन्होंने तुम्हें गंदी नज़रों से बचाकर रखा है । तुम यह सोच रही होगी कि पापा को क्या लेना-देना जब वह लड़की का पैदा होना ही पसंद नहीं है, तुम्हें पता है… दुखी ज़रुर हुए थे जब तुम पैदा हुई थी । धीरे-धीरे तुम्हारे प्यार ने ही उन्हें बदल दिया है । यह ज़रुर है कि हमारे घर में उनका शासन चलता है । घर में किसी एक शासन चलना ज़रुरी होता है । रमेश की बातें मुझे भी चुभती है फिर भी मैं सुन लेती हूं । क्यों पता है? वे हमारे लिए जीते है । क्या ज़रुरत है उनको बाहर जाकर काम करने की ? क्या ज़रुरत हैं कि वे अपना परिवार छोडकर शहर में आकर कमा रहे है? क्या उनको इतनी मेहनत करने की ज़रुरत है कि वे हमारे लिए मकान और गहने बनाये? नहीं । फिर… हमें भी समझना चाहिए । कह देना आसान है कि उनके जैसा पति नहीं चाहिए । सच बताऊँ तो उनके जैसा पति मिलना भी मुश्किल है ।
चारु अपनी माँ की बात सुनकर कहती है, अच्छा माँ यह सोच लिया जाय कि वे बहुत अच्छे है । जो भी कर रहे है, मात्र अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे है । पर माँ प्यार नाम भी कुछ होता है । जो इन्सान के लिए महत्वपूर्ण है । रोज की इस मशीन की जिंदगी में अगर कोई प्रेम से बतिया दे तो कितना अच्छा लगता है । हंमेशा चिल्लाना और सिर्फ अपनी बात को मनवाना यह भी कोई बात हुई ।
चांदनी भी सोचते हुए कहती है, हां बिटिया, लगता तो पहले मुझे भी तुम्हारे जैसा ही था । अब हर व्यक्ति का जीने का तरीका अलग होता है । हम अगर उसे अपनाकर उनके साथ रहेंगे तो अच्छा है । वरना रोज रोते रहेंगे । अपनी ही जिंदगी से ऊब जाएंगे । रमेश हम लोगों को बहुत चाहते है, पर वह दिखाते नहीं है ।
माँ आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे आगे पढना है । मैं पापा को मनवाकर रहूंगी । आखिर मैं भी उनकी बेटी हूं । देख लेना।
रमेश के ऑफिस से लौटते ही चारु ने उनके लिए अदरकवाली चाय पेश की । रमेश ने कहा, आज क्या नई योजना हमारी बिटिया ने बनाई है ? वैसे चाय बहुत अच्छी है । अब बताइए क्या बात है ।
वो…पापा….वो …..पापा..मैं..मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ । मैं आपको वादा करती हू कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी मुझसे नहीं होगी । धीरे-धीरे कहती है, पापा मैं अपने ज़मीन की तलाश कर रही हूं । मुझे आपका सहारा चाहिए । मैंने आज तक कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया । आपने जैसा कहा वैसे करती गई । आज मैं सिर्फ अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ । सच में पापा, प्लीज। इस दुनिया में थोड़ी सी जगह चाहती हूँ । आप मेरा साथ दोगे ना पापा कहते हुए अपने घुटनों के बल चारु रमेश के पैर के पास बैठ जाती है ।
रमेश उसकी ओर देखते है फिर चांदनी की ओर । ठीक है, थोडी देर सोचकर कहते है, एक काम करना कल जाकर तुम बीएमएस वुमन्स कॉलेज का फॉम लेकर आना । अभी आखिरी तारीख बाकी है ।
चारु बहुत खुश हो जाती है और देखना पापा मैं मन लगाकर पढाई करुगी और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी । कहते हुए चारु अपनी दोस्त नीतु को फोन करके बताती है ।
चारु स्वतंत्र विचारोंवाली थी । वह अपने पैरों पर खडे होना चाहती थी । वह पढ़ाई में हमेशां से अव्वल आई है । भगवान ने जैसा रुप दिया वैसी ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी बनाया है । वह थोड़ी शरारती किस्म की थी । वह लड़कों को फेसबुक और बोट्सएप के माध्यम से उल्लू भी बनाती थी । उसे लगता था कि लोग उसे जाने और सराहे । बस उसमें एक जुनून था । उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और रमेश ने उसकी शादी एक सम्पन्न परिवार कर दी थी । उसने वहां पर अपने पति से कहा कि उसने इतनी पढाई की है अब वह पढाना चाहती है । उनके पति किरण भी उसकी बातों को स्वीकार कर लिया । यही सारी बातों को सोचते हुए चारु समुंदर के किनारे बैठी हुई छोटे पत्थरों को पानी में फेंक रही थी । मंद-मंद हवा बह रही थी, उसका आनंद ले रही थी ।
अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है । अरी ओ! चारु मैं तो पुकारकर थक गई । तुम यहाँ बैठी हो । तुम्हारा फोन कहाँ है ? मैं तो तुम्हें फोन करके भी थक गई । अब तुम चलो। कहते हुए उसका हाथ नीतु पकडती है ।
अरे! नीतु तुम ? ऐसे कैसे और क्यों? देखो न! यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है । कभी-कभी एकांत भी कितना अच्छा लगता है । देखो थोडी देर के लिए बैठोगी तो इन लहरों को भी सुन पाओगी । कहकर नीतु को भी पास बिठाती है ।
नीतु जिद्द पर अड़ी थी । उसकी जिद्द को देखकर चारु कहती है, कहाँ जाना है हमें और क्यों?
नीतु ने कहा उसे बधाई देते हुए कहा, देखो तो तुम कैसे अनजान बनी बैठी हो ? तुम्हें इतने सारे सम्मान मिले अब तो हमे पार्टी चाहिए । नीतु चारु का हाथ पकडते हुए कहती है, अच्छा अब बताओ तुम्हें किस किताब के लिए सम्मानित किया गया । मैं बहुत खुश हूँ । अगर तुम मुझे किताब का नाम बताओगी तो मैं भी उसे पढूंगी । मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है ।
अरी! वो सम्मान मुझे कोई किताब के लिए नहीं दे रहे है । वो तो मेरे प्रपत्र वाचन के लिए दे रहे है । किताब तो मैंने अभी तक नहीं छपवाई । लेकिन हम आपको पार्टी ज़रुर देंगे । कहते हुए चारु अपनी दोस्त के साथ पानी-पुरी खाने चलती है ।
पानी-पुरी खाते हुए नीतु अपनी सहेली चारु से कहती है, मैं एक बात पूछू। बुरा मत मानना । तुम्हारे जैसे कितने ही लोगों ने प्रपत्र लिखें होंगे । तो उनको क्यों नहीं सम्मानित कर रहे है ?
पानी-पुरी अच्छी है अब गोल-गप्पे खाएगी? मुझे नहीं पता कि दूसरों को क्यों नहीं सम्मानित कर रहे है ? मुझे तो इतना पता है कि वे मुझे बुलाते है और सम्मान करते है ।
नीतु उसकी ओर देख रही थी कि उसने कितनी आसानी से अपनी बात रख दी उसे बुरा तक नहीं लगा । उसके चेहरे पर कुछ भी ऐसे भाव नहीं लग रहे थे कि उसे बुरा लगा हो । नीतु यही बात सोचते हुए अपनी सहेली के साथ उसके घर जाती है । नीतु को लगता है कोई बिना कुछ किए कैसे सम्मान ले लेता है । तो क्या किसीको सम्म्मान हासिल करने के लिए कुछ लिखने की ज़रुरत नहीं है । लोग मेहनत करके कविता या कहानी या साहित्य में कुछ लिखते ही क्यों है? बस कुछ प्रपत्र लिख दिए सम्मान मिल गया ।
चारु अपनी सहेली को हिलाती है और कहती है मेमसाब घर आ गया है । क्या इतना सोच रही हो । देखो अपना दिमाग यों नाहक खराब नहीं करते । जिंदगी में कुछ बातों को ऐसे रहने में ही सबकी भलाई है ।
फिर भी चारु तुमने यह सब कितनी आसानी से कह दिया । सच बताऊँ तो सब जो प्रपत्र लिख रहे है, सबको सम्मानित करना चाहिए । तुम अकेली नहीं हो ।
थोड़ी देर के लिए चारु चुप हो जाती है । नीतु की इस बात का उसके पास कोई उत्तर नहीं था । उसने कहा ठीक अब मैं अदरकवाली चाय बनाकर लाती हूँ । तुम्हें पता है, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ । कहते हुए रसोईघर में चली जाती है ।
नीतु भी कहानी और कविता लिखती है । आज तक उसने जो भी सम्मान हासिल किया, उसकी लेखनी के लिए था । वह अपने नियमों की पक्की थी । उसे बुरा लग रहा है क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते है । सिर्फ अपना नाम कॉलेज में कमाने के लिए ऐसे सम्मान लेते है । नीतु सोच रही थी कि अचानक चारु के फोन की घंटी बजती है । चारु चाय बनाने में व्यस्त थी । नीतु ने चारु का फोन उठाया ।नीतु बताने जा रही थी कि पता चला कि उसके धर्म भाई बात कर रहे है ।
धीरज भाई साब आप? हाँ, नीतु बहिना कैसी हो? अरी! बहिना आप ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है । हमने कविता पढ़कर चयन समिति को भेजा था । उन्होंने आपको श्री श्री श्री सम्मान के चयन किया है । बाकायदा आपको पत्र भी मिल जाएगा । आप २५ मई को भोपाल में आइएगा । भोपाल में आपका स्वागत है ।
भैया, शायद पारिवारिक परेशानियों की वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी । तो क्या आप मेरा सम्मान घर पर भिजवा सकते है ? जी,बहिना मैं समिति से बात करके चारु के साथ भिजवा दूंगा । चिंता की कोई बात नहीं है । उनको भी सम्मानित किया जा रहा है । नीतु को अजीब लगा और बता दिया, कि भैया उन्होंने कोई किताब अभी तक छपवाई नहीं है और कोई कविता भी उनकी प्रकाशित नहीं हुई है । क्षमा कीजिएगा, लेकिन उनको ….मतलब….।
तो क्या हुआ बहिना कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा है । आप जानती हो वह हमारी जगह से है । फलस्वरुप उनको सम्मानित करते है । लेकिन भैया यह तो गलत तरीका ही है। मतलब जो कोई आपकी जगह् से होगा या फिर रुपया देंगे तो आप उनको सम्मानित कर देंगे । यह भी कोई बात हुई । यह तो अन्याय है । जो सच में साहित्य की रचना कर रहे है, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा । जो सच में सम्मान के योग्य है, उनके साथ तो अन्याय ही हो रहा है । हमारे यहां पर भी साहित्य की चोरी करके खुद का नाम लिख देते है । ऐसी गलत हरकतों पर मुझे बहुत गुस्सा भी आता है । लेकिन मैं अकेली क्या कर सकती हूँ । सिर्फ लिख सकती हूँ । और हम भी किन-किनको रोकेंगे । आजकल विश्वविद्यालय में अपना नाम और स्थान बनाने हेतु लोग ऐसा कर रहे है। आप भी क्या कर सकते है? भैया आपने अपना बडप्पन ही दिखाया है । अब सोचना तो उनको है जो सम्मान ऐसे हासिल कर रहे है । अच्छा, भैया इस बार तो मैं नहीं आ पाऊँगी लेकिन अगली बार अवश्य आने की कोशिश करुँगी । कहते हुए नीतु फोन रख देती है ।
चारु अपनी सहेली के लिए चाय और बिस्कुट भी लेकर आती है । नीतु का मन नहीं करता, फिर भी वह चाय पीती है । फिर कहती है आपके भाई का फोन आया था । ऐसे ही बात कर रही थी । वे मेरे भी धर्म भाई है। फिर चाय का एक घूंट पीकर कहती है, मेमसाब आपका अगला पड़ाव कहाँ पर है । चारु कहती है, अगला पडाव मैं कुछ समझी नहीं । अरे! मैं सम्मान की बात कर रही थी ।
पता नहीं । कब, कौन बुलाएगा ? पता है तुम्हें मेरे पति भी मेरे साथ आते है । उनको भी मुझे सम्मानित होते देख बहुत अच्छा लगता है ।
यह तो बहुत अच्छी बात है । तुम्हें अपने पैरों तले की ज़मीन मिल गई ना चारु। कहते हुए नीतु व्यंग्य रुप से मुस्काती है । चारु उसके व्यंग्य को न समझने का अभिनय करती है । सही कहा तुमने मुझे थोडी ज़मीन तो मिल गई ।
© डॉ. अनिता एस. कर्पूर ’अनु’
२७२, रत्नगिरि रेसिडेन्सी, जी.एफ़.-१, इसरो लेआउट, बेंगलूरु-७८